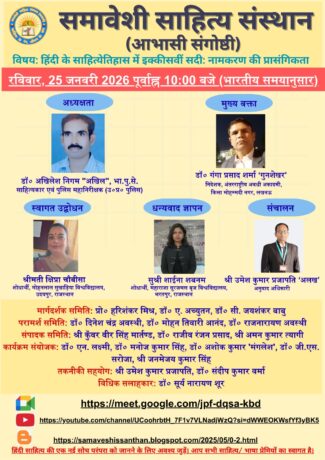बिजली, सिर्फ तारों और वोल्टेज से कहीं अधिक उत्तराखंड में विकास की बुनियाद है। यह क्लीनिक और कोल्ड चेन को ऊर्जा देती है, जो जीवनरक्षक दवाओं को सुरक्षित रखती है। यह कक्षाओं को रोशन करती है और डिजिटल शिक्षा को सहारा देती है। यह छोटे और बड़े उद्योगों की भारी भरकम मशीनरी चलाती है और कृषि, पर्यटन और सेवाओं में लोगों को आजीविका कमाने में मदद करती है। आर्थिक दृष्टि से, भरोसेमंद और सस्ती बिजली विकास को गति देती है। मानवीय दृष्टिकोण से, यह जीवनरेखा भी मानी जाती है।
लेकिन, कभी अग्रणी जलविद्युत राज्य रहने के बावजूद, उत्तराखंड अब लगातार ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। यह संकट उसकी प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है और उद्योगों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), को उत्तर प्रदेश की ओर पलायन के लिए मजबूर कर रहा है।
उद्योग क्यों जा रहे हैं?
सबसे पहला और सीधा कारण है-उद्योगों के लिए बिजली की ऊंची कीमत। उत्तराखंड का टैरिफ ढांचा भारी क्रॉस-सब्सिडी मॉडल पर आधारित है। घरेलू उपभोक्ताओं को, खासकर चुनावी वर्षों में, कृत्रिम रूप से कम दरों का लाभ मिलता है, जबकि उद्योग लगभग दोगुना भुगतान करते हैं। यह प्रणाली कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है. लेकिन वास्तव में यह ऊर्जा-गहन उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है और निवेश को हतोत्साहित करती है। MSME के लिए ₹3.25 प्रति यूनिट और ₹6.85 प्रति यूनिट का अंतर विकास और बंद होने के बीच का फर्क बन सकता है।
दूसरा, उत्तराखंड ने उद्योगिक बिजली लागत कम करने के एक बेहतरीन साधन ओपन एक्सेस को कमजोर कर दिया है, ₹1.25 प्रति यूनिट का भारी अतिरिक्त शुल्क लगाकर। ओपन एक्सेस में बड़े उपभोक्ता सीधे उत्पादकों से बिजली खरीद सकते हैं, अक्सर सस्ते दामों पर, जिससे स्थानीय वितरण कंपनी (DISCOM) को बाईपास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां ऐसे शुल्क कम हैं, उद्योग स्थिर और सस्ते बिजली अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अतिरिक्त शुल्क से इसका लाभ खत्म हो जाता है।
तीसरा, नीति की अनिश्चितता और राजनीतिक हस्तक्षेप निवेशकों के विश्वास को घटाते हैं। चुनाव से पहले टैरिफ बढ़ोतरी टाल दी जाती है, बिना दीर्घकालिक वित्तीय योजना के सब्सिडी की घोषणा हो जाती है, और पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने वाले जलविद्युत प्रोजेक्ट भी नौकरशाही या स्थानीय राजनीति में फंस जाते हैं। यह अनिश्चितता उद्योगों को जोखिम प्रिमियम जोड़ने पर मजबूर करती है, जिससे उत्तर प्रदेश का स्थिर माहौल ज्यादा आकर्षक लगता है।
चौथा, उत्तराखंड अपने प्राकृतिक जलविद्युत लाभ का पूरा उपयोग नहीं कर रहा। यहां की नदियां सस्ती और प्रचुर स्वच्छ बिजली का स्रोत हो सकती हैं, लेकिन ऊंची रॉयल्टी, जल उपयोग शुल्क और अन्य चार्ज उत्पादन लागत बढ़ाते हैं। नतीजतन, यहां का जलविद्युत, बाहर से आने वाले कोयला-आधारित बिजली से भी महंगा पड़ सकता है। यह न केवल उद्योगों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि राज्य के पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी कमजोर करता है।
पांचवां, आपूर्ति की अस्थिरता स्थिति को और बिगाड़ देती है। जलविद्युत विस्तार में रुकावट और शहरी व औद्योगिक मांग में वृद्धि के कारण, राज्य को शॉर्ट टर्म बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इससे खरीद लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जो अंततः उद्योगों पर ऊंचे टैरिफ या स्थिर शुल्क के रूप में डाल दी जाती है।
उद्योगों के जाने से होने वाला असर
रोजगार खत्म होनाः खासकर छोटे शहरों में, जहां औद्योगिक क्लस्टर गैर-कृषि नौकरियों का मुख्य स्रोत होते हैं।
राजस्व में गिरावटः जीएसटी कलेक्शन घटता है, औद्योगिक संपत्तियों से मिलने वाला प्रॉपर्टी टैक्स कम होता है, और नगर निकाय सेवा शुल्क से वंचित हो जाते हैं।
आर्थिक कड़ियों का टूटनाः उद्योग स्थानीय सप्लायर, परिवहन, मरम्मत सेवाओं और आतिथ्य व्यवसायों को सहारा देते हैं। इनके जाने से एक श्रृंखलाबद्ध व्यापार बंदी हो सकती है।
मानव विकास सूचकांकों में गिरावटः नौकरियों के अभाव में आय घटती है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर खर्च कम हो जाता है।
बुनियादी ढांचे का अनुपयोगी होनाः उद्योगों के लिए बनाए गए सड़क, बिजली लाइनें और औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़े रहते हैं।
इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश को इन सबका फायदा मिलता है-अधिक नौकरियां, व्यापक औद्योगिक टैक्स बेस, मजबूत सप्लाई चेन और निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल।
क्या बदलना होगा?
1. टैरिफ का तर्कसंगतीकरण
० क्रॉस-सब्सिडी खत्म करें जो उद्योगों को नुकसान पहुंचाती है।
गरीब परिवारों को लक्षित सहायता दें, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
निष्पक्ष और पूर्वानुमानित टैरिफ उद्योगों को दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने में मदद करेंगे।
2. ओपन एक्सेस में सुधार
० अतिरिक्त अधिभार को वास्तविक लागत के अनुरूप करें।
इससे बडे उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली खरीदना संभव होगा।
3. जलविद्युत को प्रतिस्पर्धी बनाना
० रॉयल्टी और टैक्स संरचना सरल करें।
छोटे हाइड्रो, पंप्ड स्टोरेज और हाइब्रिड नवीकरणीय प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाएं।
4. ऊर्जा नीति का राजनीतिकरण खत्म करना
० बहुवर्षीय टैरिफ और खरीद योजनाएं बनाएं, जो चुनाव चक्र से प्रभावित न हों।
5. MSME को सीधा समर्थन
० कम टैरिफ या समय-आधारित छूट दें।
० ऊर्जा दक्षता और साझा नवीकरणीय प्रोजेक्ट के लिए ऋण उपलब्ध कराएं।
6. आपूर्ति स्थिरता में सुधार
ग्रिड अपग्रेड करें, ऊर्जा स्रोत विविध बनाएं, और दीर्घकालिक नवीकरणीय अनुबंध करें।
7. पारदर्शी संवाद को बढ़ावा देना
नियमित रूप से टैरिफ संरचना और ओपन एक्सेस डेटा साझा करें।
उद्योग-DISCOM कार्य समूह बनाएं।
सशक्तिकरण बनाम क्षरण का फैसला
उत्तराखंड का मौजूदा रास्ता उसके औद्योगिक आधार और विकास की नींव को कमजोर कर रहा है। हर फैक्ट्री का बंद होना या जाना सिर्फ आंकड़ा नहीं है यह एक युवा की नौकरी खोना, एक परिवार की आय घटना और एक कस्बे के भविष्य का धुंधला होना है।
बिजली नीति इसमें बड़ा योगदान देती है। अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया, तो उद्योग और उनके लाभ पड़ोसी राज्यों की ओर चले जाएंगे। लेकिन अगर सही तरीके से संभाला गया, तो बिजली फिर से आर्थिक और मानव विकास की ताकत बन सकती है।
राज्य के पास दो विकल्प हैं-या तो वह दूरदर्शी ढांचा अपनाए, जो न्यायपूर्ण मूल्य निर्धारण करे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को उजागर करे और उद्योगों को विकास के साझेदार के रूप में देखे, या फिर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लेकिन
आर्थिक रूप से हानिकारक ऊर्जा मॉडल पर कायम रहे।
अगर साहसिक कदम उठाए जाएं, तो राज्य औद्योगिक पलायन रोक सकता है, नया पूंजी निवेश आकर्षित कर सकता है और अपनी नदियों को सतत समृद्धि व प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक बना सकता है।
हालांकि सरकार सौर ऊर्जा सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

~ स्नेह यादव
snehy879@gmail.com
डिस्क्लेमरः इस लेख में लेखक स्नेह यादव व्यक्तिगत चिार हैं। इसके साथ opendoornews.in की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेखक की ही होगी।
प्रतीक चित्र- अंतरजाल से साभार